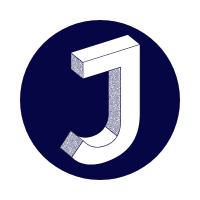Victim/hin
To view in English click here
'पीड़ित' क्या है
पीड़ित वह व्यक्ति है जो किसी विनाशकारी या हानिकारक कार्य या एजेंसी से पीड़ित होता है।[1] इसके अतिरिक्त, पीड़ित वह व्यक्ति है जो या तो किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के कार्यों के कारण, या बीमारी या संयोग के कारण आहत हुआ है या पीड़ित हुआ है।[2]
पीड़ित की आधिकारिक परिभाषाएं
विधानों में परिभाषित
पीड़ित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 2(य) (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2(वा)) पीड़ित को इस प्रकार परिभाषित करती है - "पीड़ित" का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे किसी ऐसे कार्य या लोप के कारण कोई हानि या क्षति हुई है जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है और इसमें ऐसे पीड़ित का संरक्षक या विधिक उत्तराधिकारी भी शामिल है; यह परिभाषा व्यापक है और उसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जो उस कृत्य या चूक के कारण चोट या हानि झेल रहा है, जिसके लिए आरोपी पर आरोप लगाया गया था, जिसमें उनका अभिभावक और कानूनी उत्तराधिकारी भी शामिल हैं।
आधिकारिक दस्तावेजों में परिभाषित पीड़ित
अपराध और शक्ति के दुरुपयोग के पीड़ितों के लिए न्याय के मूल सिद्धांतों की घोषणा, 1985[3] पीड़ितों को इस प्रकार परिभाषित करती है - "वे व्यक्ति जो, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, हानि से पीड़ित हुए हैं, जिसमें शारीरिक या मानसिक चोट, भावनात्मक पीड़ा, आर्थिक हानि या उनके मौलिक अधिकारों का महत्वपूर्ण हनन शामिल है, जो सदस्य राज्यों में लागू आपराधिक कानूनों का उल्लंघन करने वाले कृत्यों या लोपों के माध्यम से हुआ है, जिसमें शक्ति के आपराधिक दुरुपयोग को प्रतिबंधित करने वाले कानून भी शामिल हैं।
घोषणा आगे स्पष्ट करती है कि, "इस घोषणा के तहत, कोई व्यक्ति पीड़ित माना जा सकता है, चाहे अपराधी की पहचान की गई हो या नहीं, उसे गिरफ्तार किया गया हो या नहीं, अभियोजित किया गया हो या दोषसिद्ध किया गया हो, और अपराधी और पीड़ित के बीच पारिवारिक संबंध की परवाह किए बिना। 'पीड़ित' शब्द में, जहां उपयुक्त हो, प्रत्यक्ष पीड़ित के तत्काल परिवार या आश्रित और वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो संकट में पीड़ितों की सहायता करने या पीड़न को रोकने में हस्तक्षेप करते समय हानि से पीड़ित हुए हैं।
दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2008 ने संयुक्त राष्ट्र घोषणा के प्रभाव और मलीमथ समिति के प्रयासों के फलस्वरूप 'पीड़ित' की नई परिभाषा प्रस्तुत की। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि 2008 से पहले, पीड़ित की कोई परिभाषा नहीं थी। कानून का ध्यान पीड़ितों पर नहीं था। संयुक्त राष्ट्र घोषणा के भीतर 'पीड़ितों' की परिभाषा की तुलना में यह परिभाषा दृष्टिकोण में संकीर्ण प्रतीत होती है।
संयुक्त राष्ट्र घोषणा दो स्थितियों में किसी व्यक्ति को पीड़ित मानती है, नामतः (i) अपराध के पीड़ित और (ii) शक्ति के दुरुपयोग के पीड़ित। पहली श्रेणी उन मामलों को कवर करती है जहां चोट किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पहुंचाई जाती है जबकि पीड़न की दूसरी श्रेणी राज्य की कार्रवाई का परिणाम है। लेकिन खेद है कि हमारा ध्यान दूसरी श्रेणी की बजाय केवल पहली श्रेणी पर ही केंद्रित प्रतीत होता है।अपराध और शक्ति के दुरुपयोग के पीड़ितों के लिए न्याय के मूल सिद्धांतों की घोषणा (जीए 40/34)[4] न्याय तक पहुंच, प्रतिस्थापन, मुआवजे और शक्ति के दुरुपयोग से संरक्षण के पीड़ितों के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश प्रदान करती है:
पीड़ितों के साथ करुणा और उनकी गरिमा के प्रति सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। वे न्याय के तंत्र तक पहुंच और त्वरित निवारण के हकदार हैं, जैसा कि राष्ट्रीय कानून द्वारा प्रदान किया गया है, उनके द्वारा सहन की गई हानि के लिए। न्यायिक और प्रशासनिक तंत्र जहां आवश्यक हो स्थापित और सुदृढ़ किए जाने चाहिए ताकि पीड़ित औपचारिक या अनौपचारिक प्रक्रियाओं के माध्यम से निवारण प्राप्त कर सकें जो त्वरित, निष्पक्ष, किफायती और सुलभ हों। पीड़ितों को ऐसे तंत्रों के माध्यम से निवारण प्राप्त करने के उनके अधिकारों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। विवादों के समाधान के लिए अनौपचारिक तंत्रों, जिनमें मध्यस्थता, विवाचन और परंपरागत न्याय या स्वदेशी प्रथाएं शामिल हैं, का उपयोग जहां उपयुक्त हो किया जाना चाहिए ताकि पीड़ितों के लिए समाधान और निवारण को सुविधाजनक बनाया जा सके। अपराधियों या उनके व्यवहार के लिए जिम्मेदार तीसरे पक्षों को, जहां उपयुक्त हो, पीड़ितों, उनके परिवारों या आश्रितों को उचित प्रतिस्थापन करना चाहिए। पर्यावरण को पहुंची गंभीर क्षति के मामलों में, यदि आदेशित किया जाए तो प्रतिस्थापन में जहां तक संभव हो पर्यावरण का पुनर्स्थापन, बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण, सामुदायिक सुविधाओं का प्रतिस्थापन और पुनर्वास के खर्चों की प्रतिपूर्ति शामिल होनी चाहिए, जब भी ऐसी क्षति के परिणामस्वरूप किसी समुदाय का विस्थापन होता है। जब अपराधी या अन्य स्रोतों से मुआवजा पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, राज्यों को वित्तीय मुआवजा प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए: (क) पीड़ित जिन्होंने गंभीर अपराधों के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण शारीरिक चोट या शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य की हानि सहन की है; (ख) परिवार, विशेष रूप से उन व्यक्तियों के आश्रित जो ऐसे पीड़न के परिणामस्वरूप मृत हो गए हैं या शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गए हैं। पीड़ितों को सरकारी, स्वैच्छिक, समुदाय-आधारित और स्वदेशी माध्यमों से आवश्यक सामग्री, चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सहायता प्राप्त होनी चाहिए। पीड़ितों को स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता और अन्य प्रासंगिक सहायता के बारे में सूचित किया जाना चाहिए और उन्हें इन तक तत्काल पहुंच प्रदान की जानी चाहिए।
सरकारी रिपोर्ट में पीड़ित की परिभाषा
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई 'यौन हिंसा के उत्तरजीवी/पीड़ितों की चिकित्सा-कानूनी देखभाल के लिए दिशानिर्देश और प्रोटोकॉल'[5] नामक सरकारी रिपोर्ट, पीड़ित को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जिसे नुकसान पहुंचा है, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जो गैर-सहमति वाले यौन कृत्य के अधीन हैं, जो यौन उत्पीड़न, बलात्कार या यौन हिंसा हो सकती है। इसका यह भी अर्थ है कि एक व्यक्ति को करुणा, देखभाल, मान्यता और सहायता की आवश्यकता होती है।
154वें विधि आयोग की रिपोर्ट (1996) ने "न्याय वितरण प्रणाली में पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता को संबोधित किया और सिफारिश की कि अपराध की कुल प्रतिक्रिया में अपराध पीड़ितों की आवश्यकताओं और अधिकारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए"। रिपोर्ट में यह भी नोट किया गया था कि "वर्तमान में, पीड़ित अपराध में सबसे बुरी तरह से पीड़ित हैं और उनकी अदालती कार्यवाही में बहुत कम भूमिका होती है। उन्हें कुछ अधिकार और मुआवजा दिया जाना चाहिए, ताकि आपराधिक न्याय प्रणाली में कोई विकृति न हो।
न्यायमूर्ति मलीमथ समिति रिपोर्ट (2003) ने 'पीड़ितों के लिए न्याय' और पीड़ित-विज्ञान को सुधार के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया और सिफारिशें कीं, जो पीड़ितों की भागीदारी भूमिका बढ़ाने और बेहतर क्षतिपूर्ति न्याय पर केंद्रित थीं। इन सिफारिशों को दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 ('संशोधन अधिनियम') जैसे संशोधनों के माध्यम से शामिल किया गया, ताकि पीड़ितों के अधिकारों के मौजूदा ढांचे को मजबूत किया जा सके।
यदि पीड़ित की मृत्यु हो गई है, तो उसका कानूनी प्रतिनिधि प्रत्येक आपराधिक कार्यवाही में एक पक्षकार के रूप में चुनौती देने का अधिकार रखेगा, जहां अपराध सात वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडनीय है; चयनित मामले में, न्यायालय की उचित अनुमति से, एक स्वीकृत स्वैच्छिक संगठन को भी न्यायालय की कार्यवाही में पक्षकार बनने का अधिकार होगा; पीड़ित को एक अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व का अधिकार है और यदि पीड़ित वकील का खर्च नहीं उठा सकता है, तो राज्य पर अभियोजक प्रदान करने का दायित्व है; आपराधिक परीक्षण में पीड़ित के भाग लेने के अधिकार में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार; गवाहों से प्रश्न पूछने का अधिकार; जांच की स्थिति से अवगत होने का अधिकार, जमानत और अभियोजन की वापसी से संबंधित मुद्दों पर सुने जाने का अधिकार; और अभियोजक की दलीलों के बाद तर्क प्रस्तुत करने का अधिकार शामिल होगा; आरोपी की रिहाई, कम गंभीर अपराध के लिए सजा, अपर्याप्त सजा, या अपर्याप्त मुआवजा देने के किसी भी प्रतिकूल आदेश के खिलाफ अपील की ओर झुकने का अधिकार; पीड़ितों को कानूनी सेवाओं का विस्तार मनोचिकित्सीय और चिकित्सा सहायता, अंतरिम मुआवजा, और द्वितीयक पीड़न से संरक्षण तक किया जा सकता है; यह पीड़ित मुआवजा कानून का सुझाव देता है, जिसका प्रशासन विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीड़ित मुआवजा कोष प्रदान करने के संबंध में किया जाएगा।
पीड़ितों के अधिकारों से संबंधित कानूनी प्रावधान
वैधानिक अधिकार
- बीएनएसएस की धारा 18(8) (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24(8)) के तहत पीड़ित को अभियोजन की सहायता के लिए अपनी पसंद का अधिवक्ता नियुक्त करने की अनुमति है। हालांकि, अधिवक्ता की शक्तियां सीमित हैं, और वह केवल साक्ष्य दर्ज होने के बाद ही लिखित तर्क प्रस्तुत कर सकता है, जब तक कि न्यायालय अनुमति न दे।
- बीएनएसएस की धारा 173 (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के चरण में पीड़ित को दर्ज की गई सूचना की प्रति तुरंत, निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार है।
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64 से 71 और 74 से 79 और 124 के अंतर्गत आने वाले अपराधों के मामलों में पीड़ित का बयान एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए।
- यदि पीड़ित अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग है, तो ऐसी जानकारी पीड़ित के निवास पर या पीड़ित की पसंद के सुविधाजनक स्थान पर और एक दुभाषिया या विशेष शिक्षक की उपस्थिति में दर्ज की जानी चाहिए।
- बीएनएसएस की धारा 173 के अनुसार, पीड़ित इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से भी सूचना दे सकता है और इसे पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचनादाता द्वारा सूचना देने के तीन दिन के भीतर हस्ताक्षर किए जाने पर रिकॉर्ड में लिया जाएगा।
- यदि प्रभारी अधिकारी पीड़ित द्वारा दी गई ऐसी जानकारी को दर्ज करने से इनकार करता है, तो इसे संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेजा जा सकता है और यदि जानकारी तब भी दर्ज नहीं की जाती है, तो पीड़ित मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है।
- यदि पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी मामले को बंद करते हुए अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का चयन करता है, तो पीड़ित/सूचनादाता को बंद होने की सूचना देते हुए एक नोटिस जारी किया जाना चाहिए। बीएनएसएस की धारा 339 (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302) के तहत न्यायालय पीड़ित की ओर से एक अधिवक्ता को अभियोजन चलाने की अनुमति दे सकता है।
- पीड़ित को बीएनएनएस की धारा 413 (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372) के तहत न्यायालय द्वारा आरोपी को बरी करने या कम गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराने या अपर्याप्त मुआवजा लगाने के आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है।
- न्यायालय सजा देते समय, जिसमें जुर्माना शामिल नहीं है, निर्णय पारित करते समय, आरोपी को बीएनएसएस की धारा 395 (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357) के तहत पीड़ित (वह व्यक्ति जिसे उस कृत्य के कारण कोई हानि या चोट पहुंची है जिसके लिए आरोपी को सजा दी गई है) को मुआवजे के रूप में आदेश में निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने का आदेश दे सकता है। उसी मामले से संबंधित किसी अन्य बाद के वाद में मुआवजा देते समय, न्यायालय बीएनएसएस की धारा 395 के तहत मुआवजे के रूप में भुगतान की गई या वसूल की गई किसी भी राशि को ध्यान में रखेगा। न्यायालय बीएनएसएस की धारा 350 (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 312) के तहत न्यायालय के समक्ष किसी जांच या परीक्षण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए उपस्थित होने वाले शिकायतकर्ता/पीड़ित के उचित खर्चों के भुगतान का भी आदेश दे सकता है।
- विशिष्ट अपराधों में पीड़ित और उसकी पहचान की सुरक्षा के उद्देश्य से बीएनएसएस के तहत बंद कमरे में कार्यवाही की अनुमति है। बीएनएस, 2023 की धारा 64 से 68 और धारा 70 और 71, और यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4,6,8 या धारा 10 के तहत अपराधों का विचारण बीएनएसएस की धारा 366 (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 327) के तहत एक महिला न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा बंद कमरे में किया जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 154 और 155 (भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 151 और 152) के तहत, न्यायालय को उन प्रश्नों को प्रतिबंधित करने की शक्ति है जिन्हें वह अश्लील या बदनामी करने वाला मानता है और जो पीड़ितों और अन्य गवाहों को अपमानित या परेशान करने के इरादे से पूछे जाते हैं।
- अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 15A प्रावधान करती है कि पीड़ितों, उनके आश्रितों और गवाहों को किसी भी प्रकार के भय, दबाव, प्रलोभन, हिंसा या हिंसा की धमकी से सुरक्षा की व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य और जिम्मेदारी होगी। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करता है कि पीड़ित के साथ निष्पक्षता, सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाए और पीड़ित की आयु, लिंग, शैक्षिक कमी या गरीबी के कारण उत्पन्न होने वाली किसी विशेष आवश्यकता का उचित ध्यान रखा जाए। पीड़ित के आश्रितों के संबंध में, यह प्रावधान करता है कि उन्हें सुनवाई और अपील के बारे में न्यायालय से नोटिस प्राप्त करने का अधिकार है, और अधिनियम के तहत जमानत, रिहाई, पैरोल, दोषसिद्धि या आरोपी की सजा या किसी संबंधित कार्यवाही या तर्कों के संबंध में किसी भी कार्यवाही में सुने जाने और दोषसिद्धि, बरी या सजा पर लिखित प्रस्तुति दाखिल करने का अधिकार है।
- किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 74 यह निर्धारित करती है कि "किसी भी जांच, अन्वेषण, न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में किसी भी समाचार पत्र, पत्रिका, समाचार-पत्र, दृश्य-श्रव्य माध्यम या संचार के अन्य रूपों में कोई रिपोर्ट, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक या देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक या अपराध के बाल पीड़ित या गवाह, जो ऐसे मामले में शामिल हो, का नाम, पता या विद्यालय या कोई अन्य विवरण, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसकी पहचान की ओर ले जाए, प्रकट नहीं करेगी, और न ही ऐसे किसी बालक का चित्र प्रकाशित किया जाएगा।
- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012[6] बाल पीड़ितों की पहचान की सुरक्षा और उन्हें हुए किसी शारीरिक या मानसिक आघात या तत्काल पुनर्वास के लिए निर्धारित किए जाने वाले मुआवजे के भुगतान का प्रावधान करता है। धारा 23 बाल पीड़ित के बारे में रिपोर्टिंग (ऐसे तरीके से जो उसकी प्रतिष्ठा को कम करे/उसकी निजता का उल्लंघन करे) या उसके विवरण का खुलासा करने पर रोक लगाती है। धारा 27: यदि पीड़ित बालिका है, तो चिकित्सा परीक्षण एक महिला चिकित्सक द्वारा किया जाएगा। चिकित्सा परीक्षण बालक के माता-पिता या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में किया जाएगा जिस पर बालक विश्वास या भरोसा करता है।
- धारा 36: विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि साक्ष्य अभिलेखित करते समय बालक किसी भी तरह से आरोपी के सामने न आए, साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगा कि आरोपी बालक का कथन सुनने और अपने अधिवक्ता से संवाद करने की स्थिति में हो। धारा 37: विचारण बंद कमरे में किया जाएगा।—विशेष न्यायालय मामलों का विचारण बंद कमरे में और बालक के माता-पिता या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में करेगा जिस पर बालक विश्वास या भरोसा करता है। धारा 39: पोक्सो अधिनियम के तहत बाल पीड़ितों के लिए सहायक व्यक्ति की सहायता का दावा करने के अधिकार से संबंधित महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए मॉडल दिशानिर्देश।
- धारा 37: बंद कमरे में परीक्षण किया जाएगा। विशेष न्यायालय मामलों की सुनवाई बंद कमरे में करेगा और यह सुनवाई बच्चे के माता-पिता या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में होगी, जिस पर बच्चे को विश्वास या भरोसा हो।
- धारा 39: मॉडल दिशानिर्देश। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा POCSO अधिनियम के तहत बाल पीड़ितों के लिए सहायक व्यक्ति की सहायता का दावा करने के अधिकार से संबंधित मॉडल दिशानिर्देश बनाए गए हैं।
मुआवजा
पीड़ित मुआवजे से संबंधित प्रावधानों की विस्तृत जानकारी के लिए। पीड़ित मुआवजा पर विकी पृष्ठ देखें।
न्यायिक निर्णयों में परिभाषित पीड़ित
राम फल बनाम राज्य[7] में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीड़ित की परिभाषा के दायरे पर विचार किया और यह सारांश निकाला कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2(wa) के तहत परिभाषित 'पीड़ित' में "वह व्यक्ति भी शामिल होना चाहिए जिसके मन को नुकसान पहुंचा है"। 'पीड़ित' की परिभाषा में शामिल कानूनी वारिसों को पीड़ित द्वारा सहे गए भावनात्मक नुकसान के कारण छूट नहीं दी जा सकती।
दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वीमेन्स फोरम बनाम भारत संघ[8] में, उच्चतम न्यायालय ने प्रक्रिया के हर चरण में बलात्कार पीड़ितों के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व के महत्व पर जोर दिया – पूछताछ के दौरान उसका समर्थन करने, कार्यवाही की प्रकृति समझाने, मामले के लिए उसे तैयार करने, पुलिस स्टेशन में उसकी सहायता करने और विभिन्न एजेंसियों से राहत प्राप्त करने में उसकी मदद करने के लिए।
रेखा मुरारका बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य[9] में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि "पीड़ित आपराधिक विचारण में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वकील नियुक्त कर सकता है लेकिन वकील को गवाह की जांच करने या न्यायालय में तर्क प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं हो। जिन मामलों में पीड़ित मृत है या विकृत चित्त का है, पीड़ित का नाम या उसकी पहचान निकटतम रिश्तेदार के प्राधिकार के अधीन भी प्रकट नहीं की जानी चाहिए, जब तक कि उसकी पहचान के प्रकटीकरण को न्यायोचित ठहराने वाली परिस्थितियां मौजूद न हों, जिसका निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो वर्तमान में सत्र न्यायाधीश है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB या 376E के अधीन अपराधों और पोक्सो के अधीन अपराधों से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं रखी जाएगी। यदि पीड़ित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के अधीन अपील दायर करता है, तो पीड़ित के लिए अपनी पहचान प्रकट करना आवश्यक नहीं है और अपील पर विधि द्वारा निर्धारित रीति से कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों को वे सभी दस्तावेज जिनमें पीड़ित का नाम प्रकट किया गया है, जहां तक संभव हो, एक मुहरबंद लिफाफे में रखने चाहिए और इन दस्तावेजों को समान दस्तावेजों से बदलना चाहिए जिनमें पीड़ित का नाम सभी अभिलेखों से हटा दिया गया हो जिनकी सार्वजनिक क्षेत्र में जांच की जा सकती है।
मल्लिकार्जुन कोडागली (मृतक) बनाम कर्नाटक राज्य[10]में, न्यायालय ने माना कि आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत, अभियुक्त के अधिकार पीड़ित के अधिकारों पर प्रभावी होते हैं। उच्चतम न्यायालय ने विचारण कार्यवाही में पीड़ित की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पीड़ित प्रभाव कथन के प्रस्तुतीकरण तक सीमित नहीं रखा, बल्कि किसी भी वाद में पारित प्रतिकूल आदेश के विरुद्ध अपील करने के पीड़ित के अधिकार को भी बहाल किया।" माननीय भारत का उच्चतम न्यायालय ने निपुण सक्सेना और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य[[11] में बलात्कार के वयस्क पीड़ितों और यौन शोषण के शिकार बच्चों की पहचान की सुरक्षा के प्रश्न पर विचार करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिए:
- कोई भी व्यक्ति प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया आदि में पीड़ित का नाम नहीं छाप या प्रकाशित कर सकता है या दूर से भी ऐसे किसी तथ्य का खुलासा नहीं कर सकता है जो पीड़ित की पहचान की ओर ले जा सके और जो उसकी पहचान को आम जनता के सामने लाए।
- यदि पीड़िता मृत हो या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, तब भी उसके नाम या पहचान को उसके निकटतम संबंधी की अनुमति से भी उजागर नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि ऐसे विशेष परिस्थितियाँ न हों जो पहचान प्रकट करने को उचित ठहराएं। ऐसी परिस्थितियों का निर्णय सक्षम प्राधिकारी, जो वर्तमान में सेशंस जज है, द्वारा लिया जाएगा।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB या 376E तथा POCSO अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
- यदि कोई पीड़ित भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 372 के तहत अपील दायर करता है, तो उसके लिए अपनी पहचान उजागर करना आवश्यक नहीं होगा, और अपील को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निपटाया जाएगा।
- पुलिस अधिकारियों को चाहिए कि वे उन सभी दस्तावेजों को, जिनमें पीड़िता का नाम प्रकट होता है, यथासंभव सीलबंद लिफाफे में रखें और ऐसे दस्तावेजों की प्रतियाँ तैयार करें, जिनमें पीड़िता का नाम हटा दिया गया हो, ताकि वे सार्वजनिक रूप से निरीक्षण के लिए उपलब्ध न हों।
- सभी प्राधिकारी जिन्हें जांच एजेंसी या न्यायालय द्वारा पीड़ित का नाम बताया जाता है, वे भी पीड़ित का नाम और पहचान गुप्त रखने के लिए बाध्य हैं और इसे किसी भी तरीके से प्रकट नहीं करेंगे सिवाय रिपोर्ट में जो केवल जांच एजेंसी या न्यायालय को एक मुहरबंद लिफाफे में भेजी जानी चाहिए।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 228A(2)(c) के तहत मृत पीड़ित या विकृत चित्त के पीड़ित की पहचान के प्रकटीकरण को प्राधिकृत करने के लिए निकटतम रिश्तेदार द्वारा आवेदन केवल संबंधित सत्र न्यायाधीश को किया जाना चाहिए जब तक कि सरकार धारा 228A(2)(c) के तहत कार्य नहीं करती और ऐसी सामाजिक कल्याण संस्थाओं या संगठनों की पहचान के लिए हमारे निर्देशों के अनुसार मानदंड निर्धारित नहीं करती।
- पोक्सो के तहत नाबालिग पीड़ितों के मामले में, उनकी पहचान का प्रकटीकरण केवल विशेष न्यायालय द्वारा अनुमत किया जा सकता है, यदि ऐसा प्रकटीकरण बच्चे के हित में है।
- सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से आज से एक वर्ष के भीतर प्रत्येक जिले में कम से कम एक 'वन स्टॉप सेंटर' स्थापित करने का अनुरोध किया जाता है।
संदर्भ
- ↑ Collins' Dictionary, 'Victim'https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/victim
- ↑ Cambridge Dictionary, 'Victim' https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/victim
- ↑ https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-basic-principles-justice-victims-crime-and-abuse
- ↑ https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-basic-principles-justice-victims-crime-and-abuse
- ↑ https://main.mohfw.gov.in/sites/default/files/953522324.pdf
- ↑ Protection of Children from Sexual Offences Act https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2079/1/AA2012-32.pdf
- ↑ (आपराधिक अपील 1415/2012) दिनांक 28-05-2015https://indiankanoon.org/doc/121117145/
- ↑ Delhi Domestic Working Women’s Forum v. Union of India (1995) 1 SCC 14 [15].
- ↑ आपराधिक अपील संख्या 1727/2019, विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 7848/2019, निर्णय दिनांक 20 नवंबर, 2019।
- ↑ (2019) 2 SCC 752
- ↑ रिट याचिका (सिविल) संख्या 565/2012, दिनांक 11.12.2018।